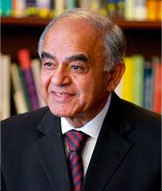
गुरचरण दास
राष्ट्र के गरीबी से सम्पन्नता की ओर जाने व एक छोर से दूसरे छोर तक फैले विचारों के संघर्ष की रोचक कहानी है. आज का भारत मुक्त बाजार-तंत्र पर आधारित है और इसने अपने हाथ विश्वव्यापी सूचना अर्थव्यवस्था में भी आजमाने शुरु कर दिए हैं.
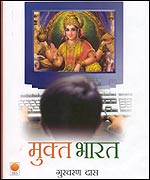
मुक्त भारत
राष्ट्र के गरीबी से सम्पन्नता की ओर जाने व एक छोर से दूसरे छोर तक फैले विचारों के संघर्ष की रोचक कहानी है. आज का भारत मुक्त बाजार-तंत्र पर आधारित है और इसने अपने हाथ विश्वव्यापी सूचना अर्थव्यवस्था में भी आजमाने शुरु कर दिए हैं. पुराना नौकरशाही राज्य, जिसने उद्योगों के विकास को दबा दिया था वह भी अब ह्रास की ओर अग्रसर है. भारत का निम्नवर्ग अब मतपेटी की ताकत के सहारे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उभर रहा है. पिछले दो दशकों में मध्यवर्ग तिगुना हो चुका है. यही आर्थिक और सामाजिक बदलाव ही इस पुस्तक का मुख्य विषय है.
इस पुस्तक में गुरचरण दास ने पिछले पचास वर्षों की आशाओं व निराशाओं को प्रस्तुत किया है. 1991 के सुनहरे ग्रीष्म के साथ ही सुधार शुरु हुए, जब शांतिप्रिय सुधारक, प्रधानमंत्री नरसिंहराव, ने आर्थिक सुधारों के साथ देश के विकास की दिशा ही बदल दी. जब सारा काम जहां राज्य के अंतर्गत होता था तब उन्होने उभरते मध्यवर्ग को आशा की एक नई किरण दिखाई, उस मध्यवर्ग को जो बाकी विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए व्याकुल था. यह एक ऐसी शांत क्रांति थी जो इतिहास में पहले कभी नही हुई थी.
गुरचरण दास ने स्वतंत्र भारत के उतार-चढ़ावों का इतिहासानुसार व अपने खुद के और सुधारों के दौरान मिले बहुत से लोगों के अनुभवों के आधार पर अध्ययन किया. यह पुस्तक नए राष्ट्र की समझ और इरादों के बारें में बताती है और कई प्रश्नों के हल खोजती है.
'मुक्त भारत आईना है
समकालीन भारत का.'
आज़ादी.मी पर गुरचरण दास के अन्य लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

